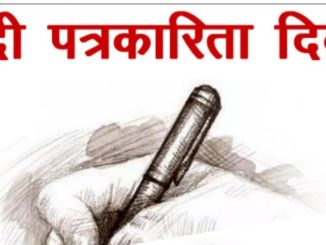विश्व मे हिन्दी इकलौती ऐसी भाषा है जिसका अशुद्ध सम्भाषण लोग के लिए हास्य का विषय है और शुद्ध वाचन भी मूर्खतापूर्ण हँसी का विषय है। ग़लत बोलने पर वक्ता का मजाक उड़ाते हैं और साहित्यिक भाषा बोलने पर उसे पाण्डित्य का प्रदर्शन कहकर उसकी अवहेलना करते हैं। हिन्दी शनैः-शनैः संकर भाषा हिंग्लिश मे रूपान्तरित हो रही है। इस स्थिति के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार वह लोग हैं जो भाषा के सम्प्रेषण मे सरलता के आदी हैं। ये मुँहचुप्पे लोग मुख खोलकर बोलने के स्थान पर केवल होंठों से बोलने का प्रयास करते हैं। हिन्दी संस्कृत की कोख से उपजी है, इसलिए इसके वाचन का ढंग वैज्ञानिक होना स्वाभाविक है। भाषा के स्वरूप पर सबसे ज्यादा सञ्चार-साधनो का प्रभाव पड़ता है। पुस्तकों, समाचार-पत्रों, टी०वी० और रेडियो की भाषा का लोग अनुकरण करते हैं। यही अनुकरण भाषाई संकरता को प्रोत्साहित कर रहा है। शब्दों का स्वरूप विकृत करना और जबरदस्ती आयातित शब्दों को भाषा-सम्प्रेषण मे कहीं भी ठूँस देने की परिपाटी ने भाषाई साम्राज्यवाद की अवधारणा को जन्म दे दिया है।
तर्कसंगत तरीके से हिन्दी का शब्द-आधार बढ़ाया जाना भाषा के हित मे है, लेकिन उसकी शुद्धता की अनदेखी हरगिज नहीं की जानी चाहिए। कोई भी भाषा, अन्य भाषाओं के बहु-प्रचलित शब्दों को खुद में समाहित करके ही जीवन्त और सामर्थ्यवान बनी रह सकती है; इस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता है। हम यह मानते हैं, यदि हिन्दी को संस्कृतनिष्ठ बनाये रखने के हिमायती लोग, अन्य भाषाओं से आये बहु-प्रचलित शब्दों को चुन-चुन कर यदि हिन्दी से निकाल बाहर करेंगे, तो वे उसे एक ऐसी भाषा बना देंगे, जिसकी सम्प्रेषण-क्षमता न्यूनतम होगी। इस देश मे जो भी बौद्धिक है, या जो गद्य या पद्य की दो-चार पङ्क्तियाँ लिखनी सीख लेता है, वह मनमानी और निरर्थक वर्तनियाँ गढ़नी शुरू कर देता है। पता नहीं ये ‘ज्ञानी’ लोग अंगरेज़ी शब्दों से छेड़छाड़ की कोशिश क्यों नहीं करते? जब लोग बोली और भाषा के बीच के अन्तर को नहीं समझते हैं तब ऐसी विकृतियाँ आना स्वाभाविक है।
ऐसे भूल जाते हैं कि बोली एक पगडण्डी की तरह है और भाषा किसी राजमार्ग की तरह। पगडंडी पर चलने वालों को नियमो (व्याकरण) से सशर्त छूट मिली है किन्तु राजमार्ग पर जरा-सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। वर्तमान मे ‘हिन्दी’ की हालत ‘गरीब की जोरू सबकी भाभी’ जैसी हो गयी है, जो भी आया मजाक करके चला गया। अज्ञानतावश, अनावश्यक और गलत शब्द गढ़ने से भाषा विकृत होती है। शब्दों और वाक्यों के बुद्धिहीन, अनावश्यक व आडम्बरपूर्ण प्रयोगों से भाषा कमजोर होती है। मीडिया मे विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज्यादातर लोग आजकल यही कर रहे हैं। अपनी भाषा-सम्बन्धी अधकचरी जानकारी को छिपाने के लिए हिन्दी को ज्यादा से ज्यादा सरल बनाने के नाम पर, गलत शब्दों को अंधाधुंध थोपने पर आमादा है। हिन्दी को तबाह करने की मुहिम में मीडिया सबसे आगे है।
हिन्दी-पत्रकारिता, भारतीय मीडिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देश की विविधता और संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। लेकिन हाल के वर्षों में, हिन्दी पत्रकारिता में भाषा के स्तर में गिरावट आयक है, जो चिन्ता का विषय है।
हिन्दी पत्रकारिता मे भाषा के स्तर में गिरावट के कई कारण हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्न हैं। अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव ने हिन्दी पत्रकारिता पर भी असर डाला है। कई पत्रकार अंग्रेजी शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करने लगे हैं, जो हिन्दी की शुद्धता को प्रभावित करता है।कई पत्रकारों को भाषा और पत्रकारिता के मूल सिद्धान्तों का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है। इससे वे अपनी खबरों में भाषा की शुद्धता बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति मे भाषा के स्तर में गिरावट भी दर्ज को जाती है। हिन्दी पत्रकारिता में भाषा के स्तर में गिरावट से हिन्दी भाषा की शुद्धता भी प्रभावित होती है। इससे भाषा के विकास और प्रसार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
पहले समाचार पत्रों की भाषा या आकाशवाणी-दूरदर्शन की भाषा को शुद्ध भाषा माना जाता था। लेकिन बढ़ते
व्यवसायीकरण के कारण वहाँ भी भाषा उपेक्षित हो गयी। देश की बुजुर्ग हो चुकी और हो रही पीढ़ी अखबारों और किताबों की परिष्कृत हिन्दी को पढ़कर भाषा-ज्ञानी बनी है। लेकिन वर्तमान पीढ़ी मीडिया से प्राप्त भाषा-ज्ञान के चलते भाषा के स्तर पर पङ्गु हो गयी है। शिक्षण संस्थानो मे भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान न दिये जाने के कारण छात्रों मे भी अशुद्ध लेखन की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
उदाहरण के रूप मे “छः” शब्द ले लीजिए। लगभग सभी समाचार पत्र और अकादमिक पुस्तकों मे इसे छह लिखा जा रहा है। आने वाली पीढ़ी इसे छह ही जानेगी और मानेगी। समाचार पत्रों मे सङ्ख्याबल को बताने के लिए भारी सङ्ख्या का प्रयोग भाषा को निचले स्तर पर ले जा रहा है। आरोपित या आरोपी, अन्तरराष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय, उज्ज्वल या उज्वल, अनधिकार या अनाधिकार, सदुपदेश या सदोपदेश, दुरवस्था या दुरावस्था, सद्गुरु या सतगुरु, द्वंद्व या द्वंद, उल्लंघन या उलंघन के साथ सैकड़ों निरर्थक और विकृत शब्दों का प्रयोग मीडिया के विभिन्न माध्यमो के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान मे मीडिया ने हँस और हंस एक कर दिये हैं। वक्ता के बोलने से ही पता चलता है कि बात क्रिया की हो रही है या पक्षी की। आधुनिकता की दौड़ मे समय के साथ अख़बारों मे जब चँद्रविन्दु, नुक़्ता या पूर्ण विराम का प्रयोग बंद हो गया, तब पाठकों ने भी उन्हें ग़ैरज़रूरी मान लिया और उदासीन हो गये।
प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और बड़े अखबार के इस शीर्षक को पढ़ें जिसमे लिखा था “सीबीएसई ने आसान की आंसर कापी रिचेक प्रक्रिया”। अब इस तरह के शीर्षक से अखबार किस भाषा मे क्या सन्देश देना चाहता है? विचार करने योग्य है!
यदि लेखन के साथ वाचन की ओर भी दृष्टि-निक्षेपण किया जाये तो स्थितियाँ और भयावह हो जाती हैं। हिन्दी पत्रकारिता मे भाषा के स्तर मे गिरावट एक गम्भीर समस्या है। हिन्दी भाषा मे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों की भरमार है। हर शब्द का अपना सौन्दर्य होता है।यदि शब्द को अपने हिसाब से तोड़-मरोड़कर, मात्राओं मे हेर-फेर कर प्रस्तुत किया जाता है तो शब्द की सुन्दरता नष्ट हो जाती है। इसके लिए पत्रकारों, अखबारों और ऑनलाइन पोर्टल्स, और पाठकों को मिलकर काम करना होगा। पत्रकारों को अपनी खबरों में भाषा की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए, अखबारों और ऑनलाइन पोर्टल्स को अपनी खबरों की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए और पाठकों को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इससे हिन्दी पत्रकारिता में भाषा के स्तर में सुधार होगा और पत्रकारिता की विश्वसनीयता बढ़ेगी।
—डॉ० राघवेन्द्र कुमार त्रिपाठी ‘राघव’, बालामऊ, हरदोई